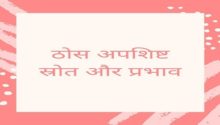Table of Contents
मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र:
उदाहरण- जीवमंडल में मनुष्य प्रमुख प्रजाति है। उन्होंने अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप पारिस्थितिकी तंत्र को संशोधित किया है। उन्होंने नए पारिस्थितिक तंत्र भी बनाए हैं। ये मानव निर्मित, या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय और जलीय हैं। स्थलीय क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी बस्तियां, वृक्षारोपण, बाग, उद्यान, पार्क, फसल भूमि और पशु फार्म शामिल हैं। मानव निर्मित जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बांध, जलाशय, झीलें, नहरें, मत्स्य टैंक, तालाब और एक्वैरिया शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र फसल भूमि हैं जिन्हें आम तौर पर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
कृषि पारिस्थितिकी तंत्र:
उत्पत्ति- मानव सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही जैविक समुदाय का संशोधन बहुत पहले शुरू हो गया था। मनुष्य ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन के लिए पौधों की खेती और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वर्तमान में, पूरी मानव आबादी कृषि पर निर्भर करती है, यानी आर्थिक पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की खेती करने की प्रथा, जिसे अक्सर फसल कहा जाता है।
मनुष्य ने वांछित फसलों की खेती के लिए जंगलों और घास के मैदानों के विशाल क्षेत्रों को फसल भूमि में बदल दिया है। फसलें मुख्य रूप से अनाज, दलहन, तिलहन और चारा हैं। चूंकि ये सभी जड़ी-बूटी वाले पौधे हैं, फसल भूमि, जिसे पशुचारण भूमि भी कहा जाता है, को चयनित वनस्पति के साथ घास के मैदान माना जा सकता है। कृषि फसलों और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कृषि पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। यह संबंध विभिन्न फसलों के साथ भिन्न होता है।
भौतिक स्थितियां- एक फसल भूमि की भौतिक स्थिति भौगोलिक स्थिति (अक्षांश और ऊंचाई), जलवायु कारकों और एडैफिक (मिट्टी) स्थितियों पर निर्भर करती है। क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल का चयन करके, उपयुक्त मौसम में इसे उगाकर और कृत्रिम सिंचाई और उर्वरकों और खादों के उपयोग से भौतिक स्थिति के संभावित प्रभावों की भरपाई की जाती है।
संयोजन- एक फसल भूमि में एक जैविक समुदाय की संरचना भिन्न होती है। प्रमुख पौधों की प्रजाति उगाई जाने वाली फसल (मोनोकल्चर) है। कुछ खरपतवार हर खेत में अपरिवर्ती उग आते हैं। क्रॉपलैंड की पशु आबादी केंचुआ, नेमाटोड, कृंतक, कीट परागणकर्ता, कुछ पक्षी और घरेलू जानवर हैं। क्रॉपलैंड जैविक समुदाय सबसे समृद्ध होता है जब उसमें फसल बढ़ रही होती है।
भेद्यता- कृषि पारिस्थितिकी तंत्र सरल और कुशल हैं। हालांकि, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की विविधता की कमी के कारण, वे अचानक जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। सूखा, कीट और रोग पूरी फसल को नष्ट कर सकते हैं। यह तब नहीं होगा जब एक खेत (बहुसंस्कृति) में एक से अधिक प्रमुख पौधों की आबादी हो।
कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लक्षण:
कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कई सामान्य विशेषताएं हैं-
(1) वे मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और इस प्रकार कृत्रिम हैं।
(2) उनका रखरखाव और विनियमन मनुष्य द्वारा किया जाता है।
(3) उनमें आत्म-नियमन की क्षमता का अभाव है।
(4) वे खाद और कृत्रिम उर्वरकों के साथ वातित, सिंचित और पोषित होते हैं। कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग से जल प्रदूषण होता है।
(5) कीटनाशकों के उपयोग से वे रोगजनकों और कीटों (कीड़े, अन्य जानवरों और खरपतवारों) से सुरक्षित रहते हैं। कीटनाशक शाकाहारी जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं। उन्हें मवेशियों और अन्य जानवरों के हमलों के खिलाफ बाड़ लगाई जाती है।
(6) उनमें प्राकृतिक मिट्टी के पोषक तत्वों के संचलन की कमी होती है, इसलिए कृत्रिम खाद की आवश्यकता होती है।
(7) उनमें स्थिरता की कमी होती है क्योंकि वे मोनोकल्चर होते हैं और उनमें विविधता नहीं होती है।
(8) वे सूखे, बाढ़, कीटों और बीमारियों से नष्ट होने की संभावना रखते हैं। इस तरह के विनाशों ने अतीत में अकाल पैदा किए हैं।
(9) कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र में उगाई जाने वाली फसलें अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक रूप से उन्नत होती हैं।
(10) मशीनों का उपयोग फसलों की बुवाई, छिड़काव और कटाई में किया जाता है।
(11) कटाई के कारण खेतों में कोई बायोमास नहीं बचता है।
(12) खेतों में राख डालने के लिए पराली जलाई जाती है। हालांकि इससे वायु प्रदूषण होता है।
संक्षेप में, कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्यों द्वारा निर्मित, विनियमित, पोषित, संरक्षित और बेहतर किए जाते हैं; विविधता, स्थिरता, पोषक तत्वों के संचलन और स्व-नियमन की कमी होती हैं ; और कटाई के कारण खेतों में कोई बायोमास नहीं बचता है।